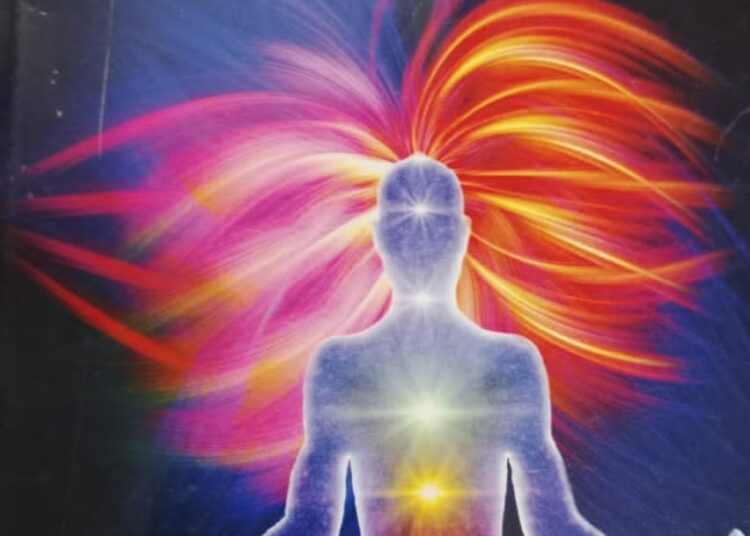श्रीनगर गढ़वाल। आज का मनुष्य जिस तेजी से भोग की ओर भाग रहा है, उतनी ही तेजी से वह भीतर से टूटता चला जा रहा है। बाहरी सुख-सुविधाओं की प्रचुरता के बावजूद मन अशांत है,विचार अस्थिर हैं और आत्मा मौन होकर कराह रही है। इसका कारण स्पष्ट है-हमने भोग को जीवन का लक्ष्य बना लिया है और योग को केवल एक क्रिया समझकर सीमित कर दिया है। जबकि सत्य यह है कि योग और भोग के संतुलन के बिना जीवन न तो स्वस्थ हो सकता है और न ही सार्थक। मनुष्य का शरीर केवल मांस,अस्थि और रक्त का ढांचा नहीं है,बल्कि वह भावनाओं,विचारों और संस्कारों का सजीव केंद्र है। जिस क्षण मन में सुख या दुख की अनुभूति जन्म लेती है,उसी क्षण उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ने लगता है। हम यह मान लेते हैं कि सुख बाहर से आता है और दुख परिस्थितियों की देन है,किंतु वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। सुख-दुख बाहर नहीं होते,वे हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं-हमारे विचारों,अपेक्षाओं और आसक्तियों से। मनुष्य स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करता। वह अपने मन की वृत्तियों को समझे बिना ही प्रतिक्रिया देता रहता है। कब,क्यों और कैसे प्रतिक्रिया करनी है-इसका विवेक जब तक विकसित नहीं होता,तब तक मनुष्य स्वयं ही अपने दुखों का निर्माता बना रहता है। आत्मा को न कोई दूसरा जान सकता है और न ही कोई बाहर से उसे मुक्त कर सकता है। आत्मज्ञान केवल आत्मदृष्टि से ही संभव है। सुख-दुख की अनुभूति वास्तव में एक मानसिक तरंग है। जो व्यक्ति इन तरंगों में बह जाता है,वह जीवन के सत्य को नहीं देख पाता। लेकिन जो साधक इन तरंगों को साक्षी भाव से देखता है-न उनसे जुड़ता है,न उनसे भागता है-वही योग के मार्ग पर अग्रसर होता है। यही योग है-चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं,बल्कि उनसे तादात्म्य का त्याग। आकाश में जैसे बादल आते-जाते रहते हैं-कभी वे विशाल पर्वत जैसे दिखते हैं,कभी पशु-पक्षियों का आकार लेते हैं-परंतु आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार हमारे हृदयाकाश में विचार,भाव और प्रतिक्रियाएं उठती हैं,आकार लेती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। हम भूल जाते हैं कि हम बादल नहीं,बल्कि आकाश हैं। हम विचार नहीं हैं,बल्कि विचारों के साक्षी हैं। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के सामने राई का दाना अत्यंत क्षुद्र प्रतीत होता है,उसी प्रकार विराट चेतना के सामने यह भौतिक संसार और इसके सुख-दुख तुच्छ हैं। किंतु हमारी दृष्टि सीमित है,इसलिए हम क्षणिक को ही शाश्वत मान लेते हैं। चित्त में उठने वाली वृत्तियां ही हमारे देखने,समझने और निर्णय लेने की दिशा तय करती हैं। वास्तव में हम संसार को नहीं देखते,बल्कि अपनी ही मानसिक अवस्था का प्रतिबिंब देखते हैं। यदि चित्त में क्रोध है,तो संसार शत्रु प्रतीत होता है। यदि भीतर भय है,तो हर परिस्थिति संकट लगती है। और यदि मन शुद्ध,शांत और प्रेम से भरा है,तो वही संसार करुणा और सौंदर्य से परिपूर्ण दिखाई देता है। इसीलिए कहा गया है-जैसा मन,वैसा संसार। विचार और भाव-दोनों ही चित्त के आकाश में विचरण करते हैं। जब तक हम इन्हें ही अपना स्वरूप मानते रहेंगे,तब तक हम बंधन में रहेंगे। योग का अर्थ संसार से भागना नहीं है,बल्कि संसार में रहते हुए उससे मुक्त होना है। भोग का त्याग नहीं,भोग के प्रति आसक्ति का त्याग ही योग है। विचाराकाश के पार जो तत्व स्थित है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। वही शुद्ध चेतना है,जो न जन्म लेती है,न मरती है। ब्रह्म विद्या केवल ग्रंथों में नहीं,बल्कि शिष्य के हृदय में प्रकट होती है। गुरु केवल मार्ग दिखाता है,चलना शिष्य को स्वयं पड़ता है। श्रद्धा,विवेक और साधना-यही उस यात्रा के आधार स्तंभ हैं। पिता की वाणी भी तभी सार्थक होती है, जब पुत्र उसे श्रद्धा और आत्मीयता से ग्रहण करे। इसी प्रकार जीवन स्वयं हमारा गुरु है। प्रत्येक अनुभव,प्रत्येक पीड़ा और प्रत्येक आनंद हमें भीतर की ओर मोड़ने का संकेत देता है। जो इन संकेतों को समझ लेता है,वही भोग से ऊपर उठकर योग की ओर अग्रसर होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम योग को केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित न रखें,बल्कि उसे जीवन की दृष्टि बनाएं। भोग को त्यागने की नहीं,बल्कि उसे समझने और सीमित करने की जरूरत है। जब भोग पर विवेक का अंकुश और योग का प्रकाश पड़ता है,तभी जीवन संतुलित,शांत और आनंदमय बनता है। योग और भोग का समन्वय ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। यही संतुलन हमें बाह्य आकर्षण से निकालकर आत्मबोध की ओर ले जाता है-जहां न सुख का अहंकार है,न दुख का भय,केवल शांति है,चेतना है और सत्य का अनुभव है।